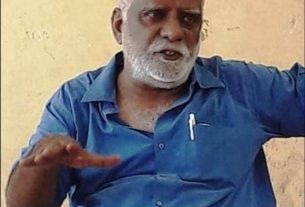संविधान और मेरा सुख –
दुख कहकर नहीं आते, इसी तरह सुख भी कहकर नहीं आते.
यहां जिस कहानी का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वह सत्य घटना है और इस कहानी को लिखने में मुझे तकरीबन पच्चीस साल लगे हैं. इस कहानी के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है.
मैंने चुनकर प्यार किया और उस प्यार के लिए मैंने सबसे अधिक कीमत अदा की.
मैं निम्न-मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आया था और मुझे जड़ सामाजिक बंधनों से नफरत थी, पिता और दूसरे रिश्तेदार चाहते थे कि मैं मथुरा के चतुर्वेदी समाज में ही शादी करूं, लेकिन चतुर्वेदी जाति का माहौल और मेरे नए जीवन मूल्य लगातार इसमें बाधा दे रहे थे, मैं चाहता था कि गैर परंपरागत शादी करूं, शादी ऐसी लडकी से करूं जो मेरी पसंद की हो और जिससे मेरे विचार और नजरिए में साम्य हो.
परंपरागत शादी में यह मुश्किल थी कि वहाँ जीवनयापन के लिए स्त्री तो मिल जाती है ,जीवन साथी नहीं मिलता! सारी दिक़्क़तें इसी वजह से पैदा हुईं.
यदि आप शादी करना चाहते हैं तो भारत में यह काम सबसे आसान है, लेकिन यदि जीवन साथी की खोज में हैं, तो यह काम सबसे मुश्किल है!
शादी का मतलब एक अदद औरत, ऐसी औरत जो शरीर सुख दे और परंपरागत घरेलू दायित्वों का निर्वाह करे, सामान्य तौर पर पति सुख के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, उसे ही हमारा समाज आदर्श स्त्री कहता है. लेकिन मैं ऐसी स्त्री एकदम नहीं चाहता था. इस तरह की स्त्री मूलत: मातहत और बंदी जीवन जीती है.
मैंने परंपरागत साहित्य और नए साहित्य के अध्ययन के बाद जो बात समझी, वह यह कि व्यक्ति को पत्नी, नहीं जीवन साथी चुनना चाहिए.
पत्नी चुनने में समाज मेहनत करता है, वही पत्नी बनाता है, जबकि जीवन साथी का चयन व्यक्ति करता है, यह दो व्यक्तियों के रसायन और पहलकदमी से बनने वाला सामाजिक संबंध है.
एक सही प्रगतिशील जीवन जीने के लिए जीवन संगिनी का जीवन साथी होना बेहद जरूरी है. जिसे समाज बेमेल विवाह कहते हैं, वह विवाह हमारी जिंदगी में पति-पत्नी के असमान संबंधों के रूप में सैंकडों सालों से जडें जमाए बैठा है.
एक सामाजिक दिक़्क़त यह भी है कि यदि आप पति-पत्नी के प्रचलित संबंध को जीवन साथी के संबंध में रूपान्तरित करना चाहें, तो सबसे अधिक प्रतिरोध औरत करती है.
यह भी देखा गया है कि पति-पत्नी संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करके, नई जिंदगी और नए रिश्ते की शुरूआत करने से हम परहेज़ करने लगते हैं और बार बार यही कहते हैं कि “लोग क्या कहेंगे, अब देखो समाज में किस तरह की बातें हो रही हैं!”
असल में “लोग क्या कहेंगे” की मनोदशा के आधार पर जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को तय नहीं करना चाहिए.
सामाजिक जीवन की नई किताब है हमारा संविधान! उसके आधार पर जीवनशैली और सामाजिक संबंधों को बार बार परिभाषित करना चाहिए.
“लोग क्या कहेंगे” की धारणा के पीछे तमाम किस्म की अतार्किकता और अविवेकवादी शास्त्र काम करता है. इसे पेट का ज्ञान कहना समीचीन होगा. पेट के ज्ञान के आधार पर हमें जीवन संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए. पेट के ज्ञान के आधार पर जो संबंध बनता है वह हमारे संविधान और नए भारत की सामाजिक -मानसिक मूल्य संरचना से बहुत कम साम्य रखता है.
संविधान में आस्था व्यक्त करने के लिए हमें जिस तरह नई राजनीति, नई सामाजिक संरचना, नए मूल्यबोध आदि को अर्जित करना पडता है, उसी तरह संविधान के आलोक में जीवन संबंधों को परिभाषित करने के लिए भी हमें नए किस्म के आंतरिक संघर्ष की जरूरत पडती है.
हम सब आंतरिक संघर्ष करने के मामले में बेहद आलसी और डरपोक हैं और आंतरिक संघर्ष करने से डरते हैं, लेकिन नए मूल्यबोध अर्जित करने लिए सामाजिक भय, आलस्य और डर से मुक्त होना बेहद जरूरी है.
मथुरा के परिवेश में रहते हुए मैंने सबसे पहली शिक्षा यह पाई कि जीना है तो संविधान के आलोक में जीवन को सँवारना होगा.
मेरे ऊपर परंपराओं और धर्म का हमेशा दवाब रहा है, आज भी है, पग पग पर परंपराएं खडी मिलती हैं, कभी मैं उनकी सुनता हूं, लेकिन मानता वही हूं वही जो संविधान कहता है.
संविधान का विवेक जीवन शैली में किस तरह रूपान्तरित करें यह आज के मनुष्य की सबसे बडी चुनौती है.
समाज को व्यक्ति के आधार पर देखने-परखने की समझ संविधान ने ही दी है, संविधान ने ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता , समानता, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि को जन जन तक पहुँचाने की समझ दी है.
यही वह बुनियादी समझ है जहाँ से मेरे युवा मन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई.
बाद में मार्क्सवाद और दूसरे ज्ञान विज्ञान के शास्त्रों ने व्यक्तित्व विकास में केन्द्रीय भूमिका अदा की.
संविधान और आधुनिक क़ानूनों की हम जब विवाद पैदा होते हैं, तब मदद लेते हैं लेकिन जीवन के विविध पक्षों का निर्माण करते समय उनकी मदद नहीं लेते.
जीवनशैली और दैनन्दिन आचरण बनाने में यदि हम संविधान और आधुनिक क़ानूनों की मदद लें तो बेहतर जीवन संबंध, बेहतर मनुष्य और प्रगतिशील समाज बना सकते हैं.
संविधान सम्मत जीवनमूल्यों पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में संविधानसम्मत चेतना का अभी तक विकास नहीं हुआ.
हमारे समाज में इसके लिए कोई मुहिम नहीं चलायी गयी.
नया समाज बनाने, नया भारत बनाने के लिए संविधान सम्मत जीवनशैली के नए रूपों और विवेकवाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है.
संविधान सम्मत और आधुनिक कानून सम्मत समझ कहती है कि शादी में दहेज न लो, लेकिन परंपरा और रीति-रिवाज की आड में यह काम खूब चल रहा है. एकबार मेरी भी चतुर्वेदी परिवार में शिक्षित कन्या से शादी की बात तकरीबन तय हो गई जन्मकुंडली मिला ली गयी, मैं राजी भी था, लडकी का परिवार शिक्षित था, लडकी भी एमए थी, मैं परिचित था उस परिवार से.
लडकी के पिता से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने साफ कहा कि मैं शादी सिविल मैरिज के रूप में करूँगा. गाजे, बाजे, बारात आदि की कोई जरूरत नहीं है. मजेदार बात यह कि मेरे पिता जो कि पंडित हैं (थे) वे सिविल मैरिज के लिए सहमत थे लेकिन लडकी के पिता जो आधुनिक शिक्षित थे, वे राजी नहीं हुए. जाहिर है ग्रह मिलने के बाद भी शादी नहीं हुई.
मेरी उस समय उम्र चौबीस साल की थी. इस घटना ने पहली शिक्षा यह दी कि मथुरा में आधुनिक संविधान सम्मत चेतना से शिक्षित समाज अभी कोसों दूर है और शादी के सवाल को परंपरा, रीति-रिवाज आदि के जरिए हल करना बहुत ही मुश्किल है.
मैंने उस समय लडकी के पिता से कहा कि जब आपके विवाद उठते हैं तो अदालत जाते हो, लेकिन शादी करने अदालत क्यों नहीं जाते ? अदालत में शादी करने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस क्यों लगती है ? संपत्ति, तलाक आदि के लिए जब अदालत की मदद लेते हो तो बेहतर यही होगा कि शादी भी अदालत में हो और बिना खर्चे के हो.
मेरे प्रस्ताव को लडकी के पिता ने ठुकरा दिया, ख़ैर मैं इस घटना के बाद बडी उलझन से मुक्त हो गया, मेरे पिता ने कहा- तुमको जो सही लगे निर्णय लो.
मैं जेएनयू पढने चला आया, इस बीच मैंने यह तय किया कि जेएनयू में पढ़ाई पूरी करने के साथ ही मन पसंद लडकी से शादी करूंगा.
मैंने जब पीएचडी जमा कर दी, और एक छोटी सी नौकरी जुगाड कर ली तो मैंने एक लडकी से अपने प्यार का इजहार किया और तय किया कि शादी उससे करूँगा.
इस संबंध को बनाने की प्रक्रिया में मैंने मध्यवर्ग का दूसरा चेहरा देखा. जिस लडकी को मैंने चुना वह देखने में सामान्य थी लेकिन शिक्षित थी, उसका बंगाली परिवार शिक्षित था, मेरे लिए इतना ही जानना जरूरी था. लडकी ने अपने पिता को पत्र लिखकर बताया कि वह मुझसे शादी करना चाहती है तो उसके माता पिता ने ज़बर्दस्त विरोध किया और कहा कि हिंदीभाषी से शादी मत करो.
लडकी अपने पिता के नजरिए को देखकर आहत हुई. वह पिता की इकलौती संतान थी इसलिए परेशानियाँ अधिक थीं , उसके पिता ने हम दोनों को बिना बताए एक व्यक्ति को कोलकत्ता से मथुरा यह जानने के लिए भेजा कि मेरे परिवार में कौन कौन हैं, मेरी शादी तो नहीं हुई है, मेरे पिता के पास कितनी संपत्ति है, वे कैसे रहते हैं घर कैसा है….उस व्यक्ति ने कलकत्ते लौटकर बताया कि लड़के के पिता की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है वह पंडित हैं.
लडकी के पिता ने तय किया कि हम दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए. लडकी अपने पिता की राय से आहत हुई और कई सप्ताह तक रोती रही.
मैंने साफ कहा कि तुमसे शादी होगी , तुम्हारे पिता कुछ भी कहें. इस पूरे प्रसंग में मेरी जाति, सामाजिक आर्थिक हैसियत को तो खंगाल लिया गया लेकिन मैंने लडकी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को खंगालने की जरूरत ही महसूस नहीं की.
मैं इस बात से परेशान था कि लड़की के पिता कम्युनिस्ट थे, वकील थे, विधायक थे, लेकिन वे भी मेरी पारिवारिक सामाजिक आर्थिक हैसियत खोज रहे थे.
मेरे लिए लडकी मुख्य थी, उसका परिवार गौण था.
अंत में मैंने तय किया कि शादी इसी लडकी से होगी उसके पिता से मैंने दो टूक शब्दों में यह बात कह दी.
लडकी के पिता ने बातचीत में तुरूप का इक्का चला और कहा कि वह जाति से शिड्यूल कास्ट है इस वजह से हो सकता है मुझे परेशानी हो, मैंने कहा जाति से नहीं, मुझे आचरण से लेना देना है. जीवन में जाति महत्वपूर्ण नहीं है आचरण महत्वपूर्ण है!
वे अंत में मेरे तर्कों से सहमत हुए, तय हुआ कि सिविल मैरिज कलकत्ते में होगी.
इस बीच मेरे जेएनयू में साथ पढ रहे मित्रों ने कहा कि मुझे यह शादी नहीं करनी चाहिए. लडकी बाद में समस्या खडी कर सकती है.
मैंने किसी की बात नहीं मानी. मथुरा में सव्यसाची जी को बताया तो बडे नाराज हुए और बोले कि चौबे होकर शिड्यूलकास्ट लडकी से शादी न करो, शादी करोगे तो मथुरा में कम्युनिस्ट पार्टी का काम करने में असुविधा होगी.
इसके विपरीत मेरे पिता ने लडकी के बारे में जानने के बाद हामी भर दी, साथ ही यह कहा कि लडकी का परिवार सही नहीं है. ख़ैर कलकत्ते में सिविल मैरिज हुई.
बाद में दो बच्चे हुए, पहले लडकी हुई, बाद में लड़का हुआ.
इस समूची जीवनयात्रा में आरंभिक दस साल बेहद तकलीफ़देह रहे, मैं घर जमाई होकर रहना नहीं चाहता था. ससुर-सास और मेरी पत्नी यही चाहती कि मैं घर जमाई होकर रहूं.
यही वह बिंदु था जहाँ से संबंध टूटने शुरू हुए. अंतत: उन्नीस साल चली कानूनी जंग में तलाक हुआ.
इस बीच उनकी ओर से जमकर कीचड़ उछाला गया, इससे मैं बहुत दुखी रहा और बार बार सोचता रहा समाज में इतने गंदे लोग क्यों हैं ? मैंने किसी का अहित नहीं किया फिर मेरे खिलाफ गंदा जहरीला प्रचार क्यों ?
मैंने समस्त प्रचार का अदालत में उत्तर दिया और अंत में मेरी जीत हुई.
मैंने उन्नीस साल कानूनी लडाई लड़कर तलाक हासिल किया. अदालत ने विभिन्न आधारों पर मेरी पत्नी को क्रूएलिटी के लिए दोषी पाया और क्रूएलिटी के आधार पर मुझे तलाक मिला.
इस समूचे दौर में जो बात महसूस की वह यह कि विपत्ति आए तो कानून की मदद लो, सामान्य जीवन में कानून का पालन करो तो कभी पराजित नहीं होगे.
बाद में मैंने दूसरी शादी सुधा सिंह से की.
इस वाक़या को लिखने का मकसद यही है कि हमारे समाज में अभी भी कानून सम्मत चेतना का अभाव है.
संविधान सम्मत जीवन शैली तमाम किस्म की सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करती है.
निदा फ़ाज़ली की यह रचना हमेशा मन में रखेः-
जब किसी से कोई गिला रखना
सामने अपने आईना रखना
यूँ उजालों से वास्ता रखना
शम्मा के पास ही हवा रखना !
घर की तामीर[1] चाहे जैसी हो
इस में रोने की जगह रखना
मस्जिदें हैं नमाज़ियों के लिये
अपने घर में कहीं ख़ुदा रखना
मिलना जुलना जहाँ ज़रूरी हो
मिलने-जुलने का हौसला रखना
शब्दार्थ:
- निर्माण, रचना